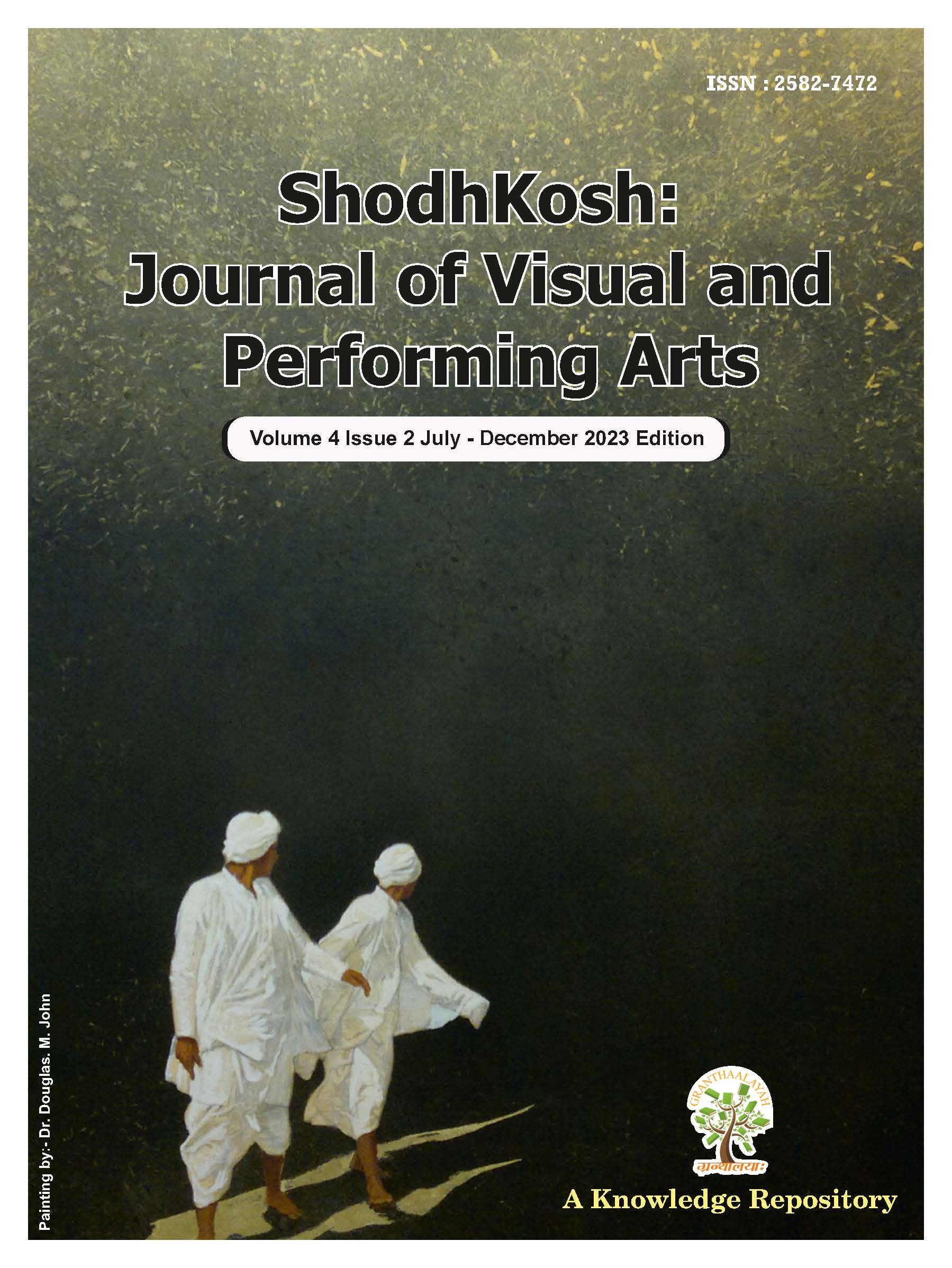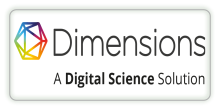DEVELOPMENT OF PRESS TRUST OF INDIA FROM PRINT TO DIGITAL AGE: HISTORICAL PERSPECTIVE
प्रिंट से डिजिटल युग तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का विकास : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
DOI:
https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.2390Keywords:
News, News Agency, Press Trust of India, PTI, API, Information Technology, SubscribersAbstract [English]
Press Trust of India (PTI) is the largest news agency of India. This news agency, which has been a companion of independent India, has a history linked to the history of colonial India and the Indian freedom struggle. This agency has its own importance due to its large network in a vast country like India. Despite the continuous changes in information technology and news gathering, how this news agency has kept itself relevant from the print age to the digital age is a subject worth knowing. Apart from technology, many challenges have come in front of news agencies in India from its inception till the present time. We will try to understand how PTI overcame those challenges through this research article.
Abstract [Hindi]
प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) भारत की सबसे बड़ी समाचार समिति/न्यूज़ एजेंसी है। स्वतंत्र भारत की सहचर रही इस समाचार समिति का इतिहास औपनिवेशिक भारत के इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा रहा है। भारत जैसे विशाल देश में अपने वृहद् नेटवर्क के कारण इस समिति का अपना महत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी और समाचार संकलन में निरंतर हुए बदलाव के बावजूद भी यह समाचार समिति अपने आप को प्रिंट युग से डिजिटल युग तक कैसे प्रासंगिक बनाए रखी है यह जानने योग्य विषय है। तकनीक से इतर भी अपनी स्थापना से लेकर वर्त्तमान कालखण्ड तक भारत में समाचार समितियों के बरक्स कई चुनौतियाँ आयीं, पीटीआई ने उन चुनौतियों से भी कैसे पार पाया यह सब कुछ हम इस शोध आलेख के जरिये समझने का प्रयास करेंगे।
References
राघवन, जी.एन.एस. (1987). पीटीआई स्टोरी: ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ़ द इंडियन प्रेस एंड द न्यूज़ एजेंसी. भारत: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया.
श्रीवास्तव, के.एम. (2007). न्यूज़ एजेंसीज : फ्रॉम पिजन टू इंटरनेट. भारत: न्यू डॉन प्रेस.
लोवेट, पैट. (1926). जर्नलिज्म इन इंडिया. भारत: द बन्ना पब्लिशिंग कंपनी.
बॉयड-बैरेट, ओलिवर. (2010). न्यूज़ एजेंसीज इन द टरब्युलेंट एरा ऑफ़ द इंटरनेट. स्पेन: कैटेलोनिया सरकार, राष्ट्रपति विभाग.
स्टोरी, ग्राहम. (1951). रॉयटर्स सेंचुरी 1851-1951. लंदन : मैक्स पर्रिश एंड कंपनी लिमिटेड.
सिल्बरस्टीन-लोएब, जोनाथन (2014). द इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ न्यूज़: एसोसिएटेड प्रेस, प्रेस एसोसिएशन और रॉयटर्स, 1848-1947. संयुक्त राज्य अमेरिका: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
स्टोरी, जी. (1951). रॉयटर्स सेंचुरी, 1851-1951, आदि [प्लेट्स के साथ, पोर्ट्रेट सहित।] यूनाइटेड किंगडम: लंदन।
जोगलेकर, काशीनाथ गोविन्दराव. (2014). संवाद समिति की पत्रकारिता. भारत: राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि.
भटनागर, डॉ. रामरतन. (2003). द राइज एंड ग्रोथ ऑफ़ हिंदी जर्नलिज्म. भारत: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय. (1977). समाचार एजेंसीयों से सम्बंधित समिति की रिपोर्ट. भारत: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.
प्रकाशन विभाग. (2022). इंडिया 2022: ए रेफरेंस एनुअल. भारत: प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार.
दास, उज्जवल चंद्र. (2016). डेवलपमेंट ऑफ़ न्यूज़ एजेंसीज: ए स्टडी ऑफ़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीएचडी थीसिस). आसाम यूनिवर्सिटी, सिलचर
Press Trust of India. About Us. https://www.ptinews.com/about से प्राप्त
Indian Media Studies. Television in India : Once an idiot box becomes 24x7 companion. https://indianmediastudies.com/television-in-india/#1991-1995_The_Dawn_of_Satellite_Television से प्राप्त
IFCN Codes of Principles. Press Trust of India. https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/application/public/press-trust-of-india/661a8b11ba7689d48142f963 से प्राप्त
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Dhirendra Kumar Rai, Harshit Shyam Jaiswal

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
With the licence CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.
It is not necessary to ask for further permission from the author or journal board.
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.